भारत एक कला और संस्कृति का देश है और शास्त्रीय नृत्य की जड़ें हमें वैदिक युग तक ले जाती हैं जब भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी जिसमें भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। भारत में आठ मुख्य शास्त्रीय नृत्य विधाओं को देखा जा सकता है। प्रत्येक नृत्य एक क्षेत्र से जुड़ा है जिसके परिवेश से उस नृत्य को वो रूप मिला जिससे हम उसे आज जानते हैं। ये आठ शास्त्रीय नृत्य हैं- भरतनाट्यम, कत्थक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओड़िसी, मणिपुरी और सत्रीया। इनमें से चार नृत्य भारत के दक्षिणी राज्यों से जुड़े हैं- भरतनाट्यम तमिलनाडू से, कुचिपुड़ी आंध्रप्रदेश से और कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से। भारत के उत्तर पूर्व में देखे जाते हैं मणिपुरी और सत्रीय। भारत के पूर्वी तटीय राज्य से आता है ओडिसी और उत्तर भारत से कत्थक। पर आप इन आठ शास्त्रीय नृत्यों से कैसे जुड़ सकते हैं? इसका जवाब भी है मेरे पास। वैसे तो इंटरनेट पर सब तरह कि जानकारी मौजूद है पर मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ जाने माने संगीत और कला से जुड़े विद्यालयों कि जानकारी, जिससे आपकी खोज थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 1- नृत्यांजलि इंस्टिट्यूट ऑफ़ परफार्मिंग आर्ट्स, मुंबई इस विद्यालय की स्थापना १९६२ में डॉक्टर तुषार गुहा द्वारा की गई थी। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था युवाओं में भारत की महान कला और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। 2- श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ़ म्यूजिक एंड डांस, हैदराबाद – १९५२ में स्थापित यह विद्यालय मुख्य रूप से कुच्चीपुड़ी नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्द है पर यहाँ शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य की ठहरा और विधाओं की शिक्षा भी दी जाती है। 3- नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, मुंबई इस स्कूल को मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ डांसिंग स्कूल्स में से एक मन जाता है। 4- कलाक्षेत्र फाउंडेशन या रुक्मिणीदेवी कॉलेज ऑफ़ फ़ाईन आर्ट्स की स्थापना भरतनाट्यम के विख्यात गुरुओं में से एक रुक्मिणी देवी जी द्वारा १९३६ में हैदराबाद में की गई थी। इस इंस्टिट्यूट को भारत सरकार द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ़ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया था। इस स्कूल में भरतनाट्यम और शास्त्रीय ...
Show More
Show Less
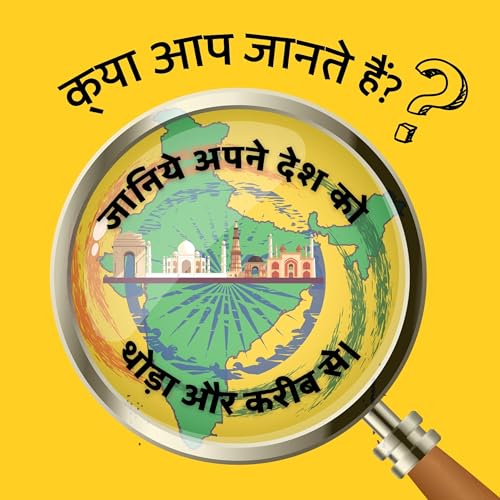 9 mins
9 mins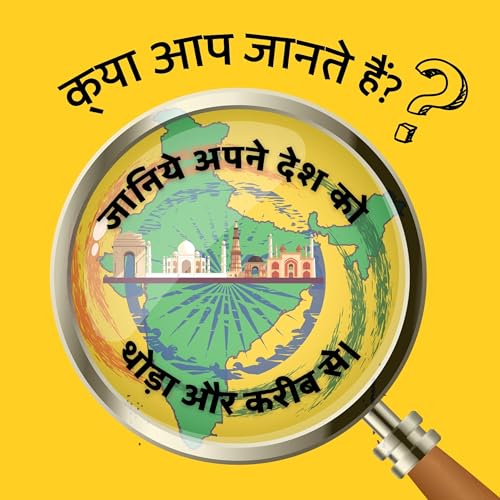 9 mins
9 mins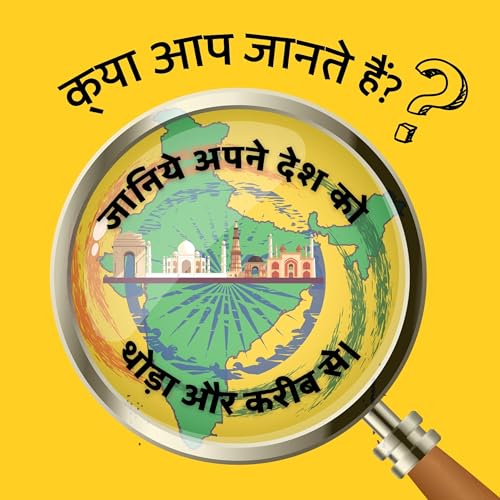 Apr 14 202311 mins
Apr 14 202311 mins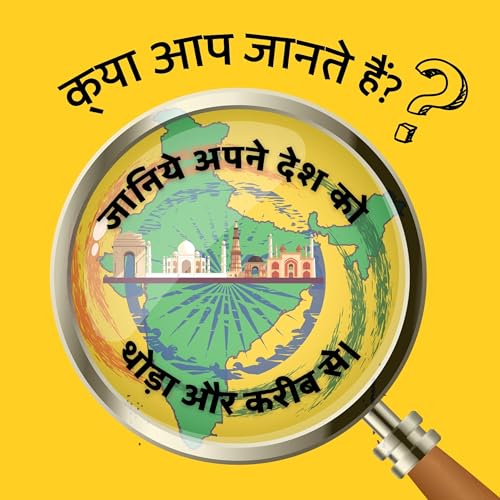 34 mins
34 mins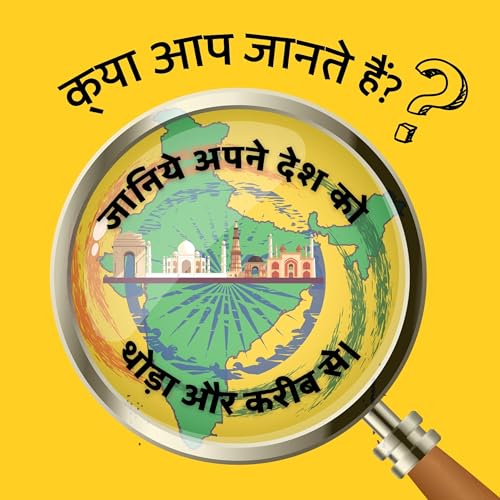 10 mins
10 mins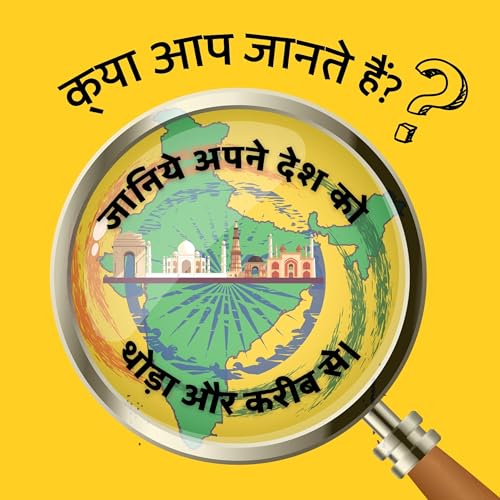
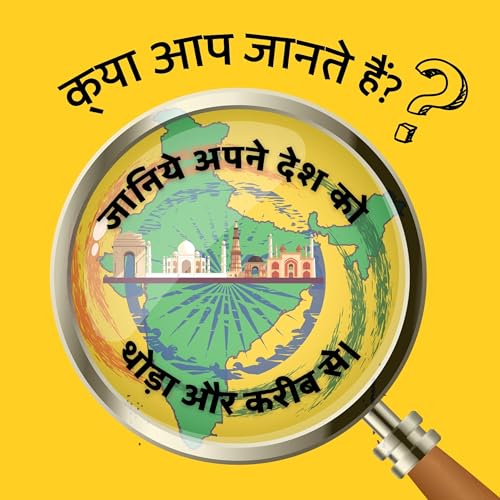 Mar 16 20236 mins
Mar 16 20236 mins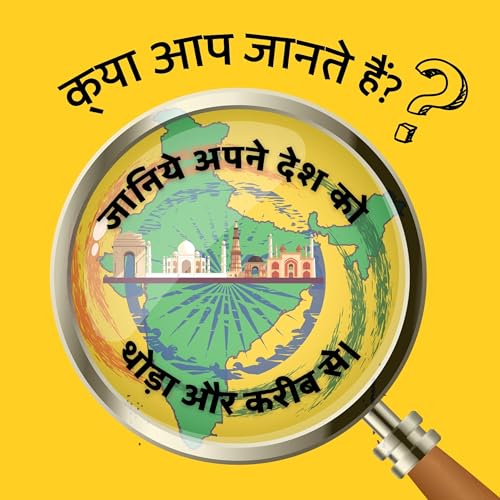 Mar 13 20236 mins
Mar 13 20236 mins
